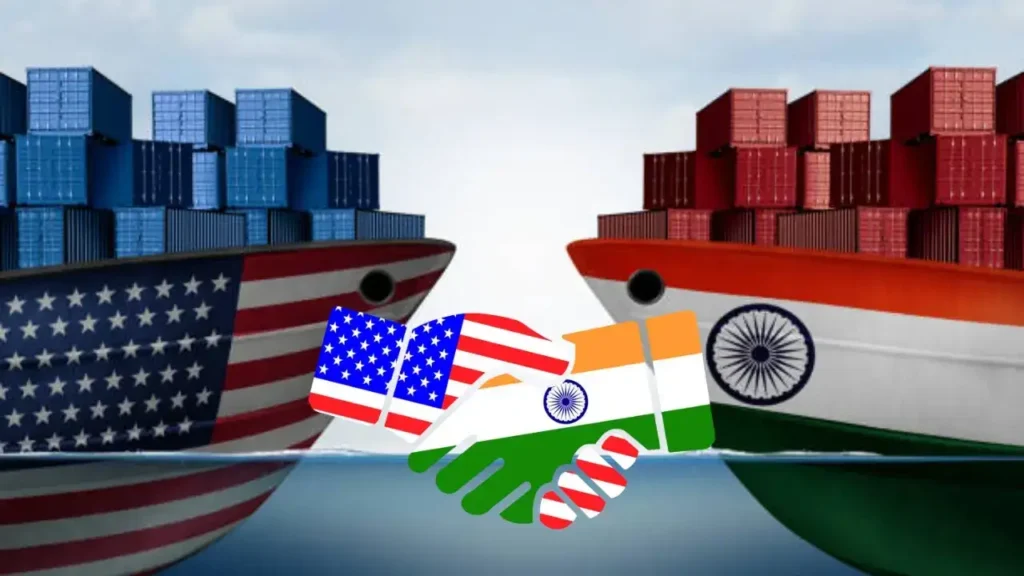भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता एक बार फिर विवादों में आ गया है। बीते कुछ वर्षों से दोनों देश इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा ने इस वार्ता को नई चुनौती में डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि यह वार्ता आखिर क्यों पटरी से उतरी, भारत ने अमेरिका को क्या प्रस्ताव दिए और आगे इस व्यापार समझौते की क्या संभावना है?
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता कब और कैसे शुरू हुई?
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद फरवरी 2017 में भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हुई। भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने अमेरिका के साथ तेजी से व्यापारिक संबंध मजबूत करने की इच्छा जताई।
इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल लगातार संवाद में बने रहे और बीते पांच महीनों में कुल पांच बैठकें भी हुईं। अप्रैल 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर आए और समझौते का एक ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया था।
भारत ने क्या प्रस्ताव दिए थे?
भारत की ओर से अमेरिका को कई बड़े प्रस्ताव दिए गए थे, जिनमें कुछ मुख्य बिंदु थे:
- औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ में छूट: भारत ने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका के औद्योगिक उत्पादों पर कोई आयात शुल्क न लगाया जाए। यह अमेरिका के कुल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा था।
- एल्कोहल और अमेरिकी कारों पर टैरिफ कटौती: भारत ने संकेत दिया कि इन दोनों सेक्टरों पर टैरिफ दरों में कमी संभव है।
- ऊर्जा और रक्षा सौदों में इजाफा: भारत ने अमेरिका को आश्वस्त किया कि वह आगामी समय में ऊर्जा और रक्षा खरीद के लिए 25 अरब डॉलर तक खर्च करेगा। इससे अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी।
फिर भी क्यों नहीं बनी बात?
हालांकि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका भारत की ओर से दिए गए प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि भारत अपने डेयरी और कृषि क्षेत्रों में भी बड़ी छूट दे, जो भारत के लिए बेहद संवेदनशील सेक्टर हैं।
दूसरी ओर, भारत को भरोसा था कि अगर वह टैरिफ में कुछ छूट देता है तो वह घरेलू किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों की रक्षा कर पाएगा। इसी खींचतान में दोनों पक्ष अंतिम सहमति तक नहीं पहुंच सके।
अमेरिका के अन्य देशों से व्यापार समझौते का क्या असर पड़ा?
जैसे-जैसे अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों जैसे वियतनाम, जापान और इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौते करता गया, ट्रंप प्रशासन की अपेक्षाएं भारत से भी बढ़ती चली गईं।
जब अमेरिका ने यूरोपीय संघ के साथ भी टैरिफ में छूट से जुड़ा करार कर लिया, तो भारत पर दबाव और बढ़ गया। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि भारत भी उसी तरह की रियायतें दे, लेकिन भारत कुछ क्षेत्रों को अपनी ‘रेड लाइन’ मानता रहा और वहां समझौता संभव नहीं हुआ।
भारत अमेरिका व्यापार समझौता के अंतिम चरण में ट्रंप क्यों नाराज़ हुए?
ट्रंप प्रशासन का मानना था कि उन्होंने अधिकांश देशों से अपने पक्ष में डील की है। वे भारत से भी वैसी ही ‘विजय’ की उम्मीद कर रहे थे।
लेकिन मई 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप ने खुद को शांति का वाहक घोषित करना शुरू कर दिया। भारत ने उनके इन बयानों को खारिज किया, जिससे ट्रंप निजी रूप से भी नाराज़ हुए। इस नाराजगी का असर व्यापार वार्ता पर भी पड़ा और बात एक बार फिर से अटक गई।
अमेरिका का नया टैरिफ: भारत पर दोहरी मार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर 25% आयात शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा। इसके ठीक बाद उन्होंने रूस के साथ व्यापार का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया, जो 27 अगस्त से लागू होगा।
इसका मतलब है कि इस महीने के अंत तक भारत से अमेरिका को जाने वाले कई उत्पादों पर कुल मिलाकर 50% तक शुल्क देना होगा, जो भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका है।
अब आगे क्या?
हालांकि, उम्मीद की किरण अभी बाकी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगस्त के मध्य में भारत आने वाला है और नई शर्तों के साथ बातचीत की उम्मीद है।
भारत की ओर से कुछ रियायतें मिलने की संभावना है:
- कृषि और डेयरी सेक्टर में सीमित छूट
- अमेरिका से तेल और गैस की खरीद बढ़ाना
- टेक और फार्मा सेक्टर में संयुक्त निवेश
विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश अब भी एक समझौते तक पहुंच सकते हैं। पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिंसकॉट का कहना है कि “दोनों देश एक समय पर काफी करीब थे और अभी भी देर नहीं हुई है।”
भारत रूस से तेल खरीदेगा , अमेरिकी दबाव में नहीं झुका
निष्कर्ष
भारत अमेरिका व्यापार समझौता मजबूत करने की कोशिशें लंबे समय से जारी हैं। हालांकि, घरेलू हितों और राजनीतिक समीकरणों के चलते यह रास्ता आसान नहीं है। फिर भी, वैश्विक मंच पर दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच बेहतर व्यापार समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।